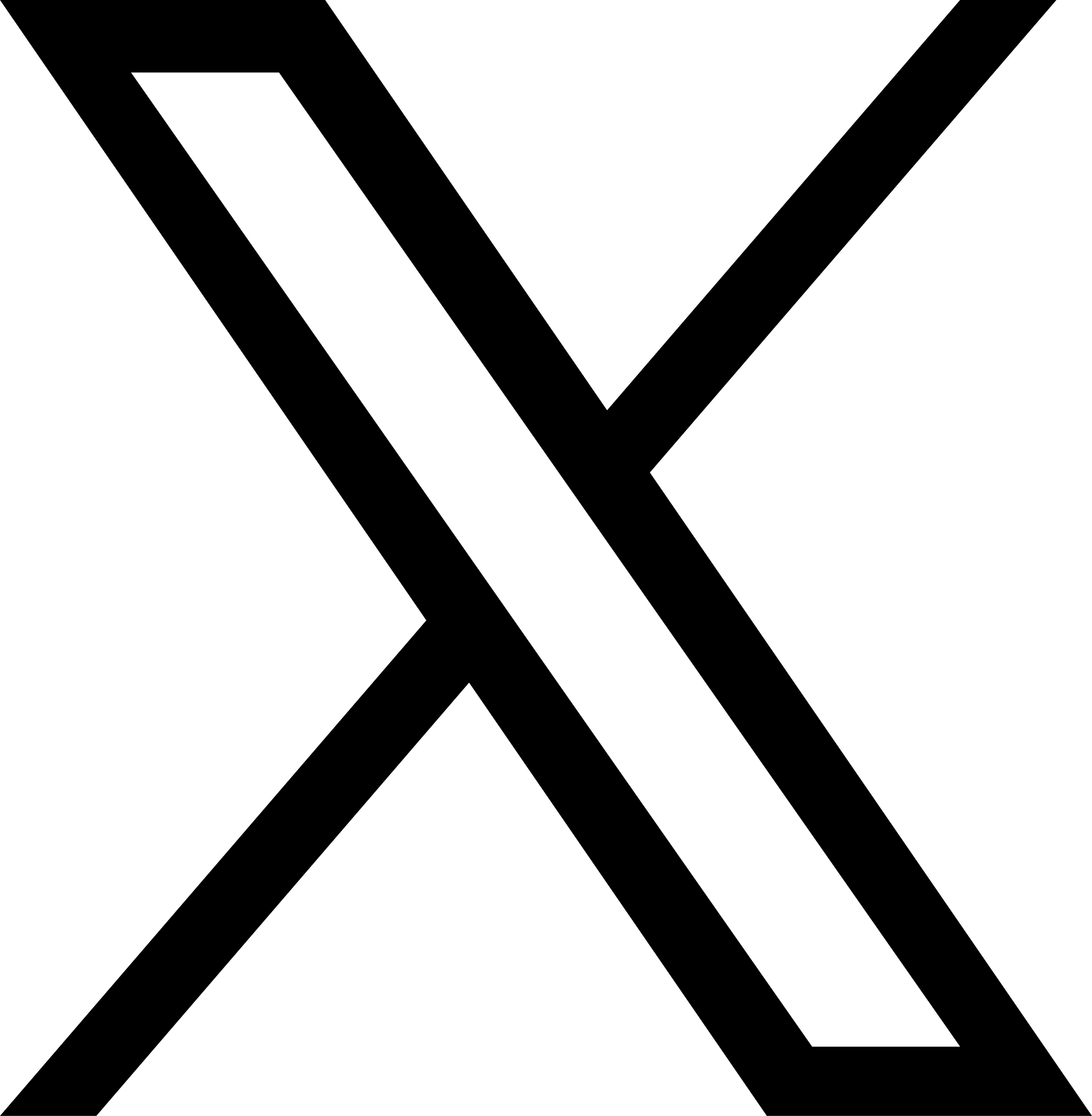सांस्कृतिक आन्दोलन की भूमिका
आज जिस दौर में हम जी रहे हैं वहां सांस्कृतिक आन्दोलन की भूमिका पर सोचते हुए इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता की एक दुसरे के पूरक दो शब्दों के निहितार्थों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता शिद्दत से महसूस होने लगी है। क्यूंकि आज सांस्कृतिकता का पूरक आन्दोलन शब्द ही हाशिये पर जा पहुंचा है । तब इस पड़ताल की आवश्यकता इस लिए बढ़ जाती है जब इन दोनों शब्दों के बीच रिक्तता की खाई को बड़ी संजीदगी से, वे बाज़ारू ताकतें अपनी चमकीली हलचलों को, सांस्कृतिक आन्दोलन बताकर, पुरे वर्गीय संघर्ष को भरमाने और पलीता लगाने में जुटी है । जब देश के बड़े माध्य वर्ग के बीच नवजागरण का स्थान दैविय जागरण ने ले लिया है और पूरा मध्य वर्ग आँखे मूंदे किसी समतामूलक समाज की कामना में तल्लीन है । ठीक उसी समय साम्प्रदायिकता का खतरनाक खेल, बाजारवाद , निजीकरण और सबसे ऊपर विकास का नाम देकर अपने संसाधनों को, कॉर्पोरेट के लिए जमकर लूटने की खुली छूट देने के उभार बैचेन करतें हैं ।
मैं निर्विकल्प होकर किसी निराशावाद से घिरे होने की बात नहीं कर रहा लेकिन, प्रेमचंद, मुक्तिबोध, कैफ़ी आज़मी, भीष्म साहनी, यशपाल, साहिर लुधियानवी, नागार्जुन, अली सरदार जाफरी, फैज़, मज़ाज़ जैसे नामों की रोशनी में खड़ा हुआ साहित्य सांस्कृतिक क्षेत्र का प्रगतिशील आन्दोलन जो एक समय में देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आन्दोलन था, जैसे किसी आन्दोलन जिससे किसी बड़े बदलाव की उम्मीद की जा सके, के बिना कोरे आशावाद से सहमत होना भी आज के दौर में कम-अज-कम तर्क संगत नहीं है।
हमेशा से ही सांस्कृतिक आन्दोलन के कुछ निश्चित लक्ष्य रहें हैं लेकिन इन आंदोलनों की सबसे बड़ी भूमिका जनमानस को एक दिशा देने की रही है । हालांकि इसका कई स्तरों पर फैलाव हुआ है लेकिन आपसी विखराव ने भी इसे कम नुकसान नहीं पहुँचाया । आज हमारे भीतर की उलझन एक और एक ग्यारह के बजाय तीन तेरह के सिद्दांत की होने लगी है । व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हमारे सांस्कृतिक आन्दोलन के सामाजिक लक्ष्यों पर भारी पड़ रही है जो न केवल उन परिवर्तनगामी बिन्दुओं को ही पीछे धकेल रही है बल्कि हमारी सामाजिक व् राजनैतिक दृष्टि भी धुंधली कर रही है । इसी का परिणाम है की आज हमारे बीच क्षणिक सांस्कृतिक प्रतिबद्धता नज़र आती है जो छोटी-छोटी महत्वाकांक्षाओं के पूरे होते ही गायब हो जाती है और फिर वही लाभ और स्वार्थों के सौदे होना शुरू हो जाता है ।

जबकि वैचारिक रूप से राजनैतिक चेतना को, लोक जनमानस की समझ के स्तर पर, सांस्कृतिक रूप से सही दिशा में ले जाने के महत्वपूर्ण सवालों के साथ, सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण से बदलाव के इस दौर में हमारे सांस्कृतिक आन्दोलन की जरूरतें हमें सांस्कृतिक आन्दोलन से भरे अतीत से सबक लेने को विवश करतीं हैं । अचम्भा नहीं है की उन्नीस सौ तीस-चालीस के दशकों की समूची भारतीय सर्जनात्मकता में इन्हीं चिंताओं के समतामूलक समाज की गूंज स्पष्ट सुनाई देती है । जिन्हें उस समय के साहित्य, कला और संस्कृति के लोग मिलकर सुत्रबद्ध तरीके से आन्दोलन का रूप देकर मुखरित कर रहे थे । हालाँकि इन आन्दोलनो से पहले कला व् साहित्य आधुनिकता से तालमेल कर चुके थे । कहानी, कविता, नाटक और फिल्मों के रूप में, लेकिन एकीकृत रूप से वे स्थानीय आम व लोक जीवन तक नहीं पहुँच पाए थे ऐसे में लोक जीवन तथा देहातों तक राजनैतिक चेतना को सांस्कृतिक आन्दोलन के रूप में पहुँचाने में इप्टा जैसे संगठनो की जो भूमिका उस समय नज़र आती है आज ऐसी सांस्कृतिक लगन और सामाजिक प्रतिवद्धता की उर्जा नज़र नहीं आती ।
ऐतिहासिक दस्तावेजों की रोशनी में यह बात स्पष्ट रूप से सामने आती है की उन सांस्कृतिक आंदोलनों का ही असर था की आम जन चेतना तक यह बात पहुँच पा रही है की स्थानीय जातीयता की बातें करने की बजाय, हमें स्थानीय सांस्कृतिक व सामाजिक मूल्यों के बचाव के लिए, एक बड़ा वैश्विक दृष्टीकोण चाहिए । चूँकि सन तीस-चालीस का दशक भी सांस्कृतिक, सामाजिक, और आर्थिक रूप से बड़े परिवर्तन का समय था । सत्ता परिवर्तन की शंका-आशंका औए सामंती व्यवस्था से जकडे ऐसे दूभर समय में, इन सांस्कृतिक आन्दोलनो का ही नतीजा था कि किसानो के बड़े संगठन बने । छात्रों के संगठन, लेखकों, कलाकारों, पत्रकारों, बुद्धेजिवियों के संगठन बने जो समाजवादी विचारधारा के प्रसार और उसी वैश्विक जनदृष्टि से पश्चिमी पूंजीवाद तथा भीतरी सामंतवाद का डटकर मुकाबला करने का स्वर प्रखर कर रहे थे । जो लेखक कलाकार पश्चिमी आधुनिकता के दवाव में बिखरकर अपनी संस्कृति से भटक रहे थे, उन्होंने भी सांस्कृतिक रूप से ग्रामीण भारत तथा लोकजन जीवन की ओर रुख किया । कहना गलत न होगा की हिंदी, उर्दू के आलावा भारत की भिन्न भाषाओं के लोक जीवन से जुडी कहानियां, नाटक, कविताएं तथा गीत, लोकगीत उसी सांस्कृतिक आन्दोलन के ताप का परिणाम था ।
बात आज की करें तो यह सवाल उठता है कि आज़ादी के बाद भी वैचारिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूप से हम आज़ाद हो पाए हैं । क्या हम पूंजीवाद और पश्चिमी सामंतवाद की जकदन से मुक्त हो पाए हैं फिर क्यूँ और किस भ्रम में हम अपने सांस्क्रतिक आंदोलनों की आग को ठंडा होते देखकर भी शांत हैं । सांस्कृतिक रूप से हमारी इसी शिथिलता का नतीजा है की हमारे पाठ्यक्रमों में से प्रेमचंद, यशपाल, परसाई, जैसे लेखकों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है । नतीजतन युवा पीढ़ी प्रतिरोध से अनिभिज्ञ है । वह भगत सिंह को राजनैतिक रूप से एक विश्वदृष्टा, समाजवादी क्रन्तिकारी के रूप में न जानकर एक आकांता के रूप में पहचान रही है । भगत सिंह की आज़ादी के माएने तथा आज़ाद भारत के समाजवादी लोकत्रंत में, सामाजिक व्यवस्था के सम्पूर्ण कार्यक्रम से यह पीढ़ी अनजान है जबकि तब ऐसा नहीं था । इसका अंदाजा भगत सिंह की उस बात से लगाया जा सकता है जो उसने फांसी से पहले अपने साथी सुखदेव से कही थी कि 'मरा हुआ भगत सिंह जीवित भगत सिंह से अधिक खतरनाक सिद्ध होगा । '
बावजूद इन स्तिथियों-परिस्थितियों के सामाजिक बदलाव की तीव्र चाहे समाज में आज भी मौजूद है, उसी स्क्रिप्ट और जूनून के साथ । इसीलिए आज ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हालातों के बाद भी सार्थक नाटकों, कविताओं, कहानियों, या फिल्मों के माध्यम से अलग-अलग जगहों पर सांस्कृतिक आंदोलनों को हवा दी जा रही है । लेकिन सांस्कृतिक धारा से ये वारिस यूँ अलग-अलग, अकेले दम पर, क्या वर्त्तमान परिस्थितियों में उत्पन्न सामाजिक चुनौतियों और उनके तकाजों की पूर्ति कर सकते हैं । फिर ऐसे हालातों में इस पर पुनर्विचार न करने का कोई कारण नहीं है । खासकर तब, जन साहित्य और कलाकर्मी, सांस्कृतिक आंदोलनों के इतिहास का पुनर्मूल्यांकन व विश्लेषण करने की दिशा में उतने सक्रिय दिखाई नहीं देते जितनी समय की आवश्यता है । मुश्किल तब और बड़ी कड़ी होती है जब ऐसी वर्कशॉप, चर्चा, परिचर्चा के दौरान हम वैचारिक रूप से सार्थक समझ परोशने के बहाने, अपने पूर्वाग्रहों, स्वनिर्मित अवधाणाओं के जरिये दबी हुइ किसी व्यक्तिगत अंतर्ग्रंथि के स्थापत्य का मौका ढूंड लेते हैं और कुछ नामों उनकी सफलता, असफलता उनके लेखन या क्रियाकलापों में सही गलत को ढूंडकर, अपना गुस्सा या भड़ास निकलकर खुद को सही साबित करने में अपना वक्त ख़राब करतें हैं । कई दफा तो हम उन्हीं राजनैतिक शक्तियों के प्रति अपनी वफ़ादारी को आच्छादित रखने को प्रगतिशीलता की प्रासंगिकता का नाटक तक रचते हैं जबकि भीतर से उन्हीं शक्तियों के प्रति आस्थावान बने रहतें हैं ।
आवश्यकता है अपनी व्यक्तिगत संकीर्णताओं को तोड़ने की, और अलग अलग विखराव में सांस्कृतिक रूप से छोटे-छोटे अन्दोलनो को खाद पानी देने में जुटे संगठनो को इतिहास से सबक लेकर, एकरूपता में सूत्रबद्ध तरीके से विभिन्न सांस्क्रतिक क्रियाकलापों के उत्साह के साथ एक बड़े सांस्कृतिक आन्दोलन की भूमिका की दिशा में प्रयासरत होने की । सोचने वाली एक और बात है कि हमारे सांस्कृतिक कर्मों में वर्तमान युवा और नयी पीढ़ी की सहभागिता न के बराबर हो गयी है । इसके पीछे छिपे कारणों की पड़ताल की आवश्यकता है । इस परिपेक्ष्य में यहाँ सज्जाद ज़ाहिर द्वारा १९३६(1936 ) में साहित्यिक सांस्कृतिक आन्दोलन की इसी विकासशीलता पर लिखा गया यह कथन ज़्यादा प्रासंगिक होगा "हम बहार से कोई अजनबी दाना लाकर अपने खेत में नहीं बो रहे थे । नए साहित्य और कला के बीज हमारे देश के ही विवेकशील बुद्धिजीवियों के मन में मौजूद थे । खुद हमारे देश की आबोहवा ऐसी हो गयी थी जिसमे नै फसल उग सकती थी । प्रगतिशील साहित्य आन्दोलन का उद्दयेश इस नयी फसल को पानी देना, इसकी निगरानी करना और इसे परवान चढ़ाना था । कमोवेश आज सार्थक सामाजिक चेतना के लिए कला साहित्य और संस्कृति के प्रति उसी एकनिष्ट लगाव, जोश, जूनून और हौंसले की जरुरत है । ताकि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाज़ार, सम्राज्यवाद और भारतीय शाशक वर्ग की देने वर्तमान सांस्कृतिक चुनौतियों का जनवादी सांस्कृतिक आन्दोलन के ज़रीए रचनात्मक जबाव दिया जा सके । और यही पूरे क्षेत्र को बदलने की क्षमता का आगाज़ होग। जो भारतीय सांस्कृतिक आन्दोलन के इतिहास के पन्नों में दर्ज है ।
Disclaimer: The views expressed here are the author's personal views, and do not necessarily represent the views of Newsclick
Get the latest reports & analysis with people's perspective on Protests, movements & deep analytical videos, discussions of the current affairs in your Telegram app. Subscribe to NewsClick's Telegram channel & get Real-Time updates on stories, as they get published on our website.